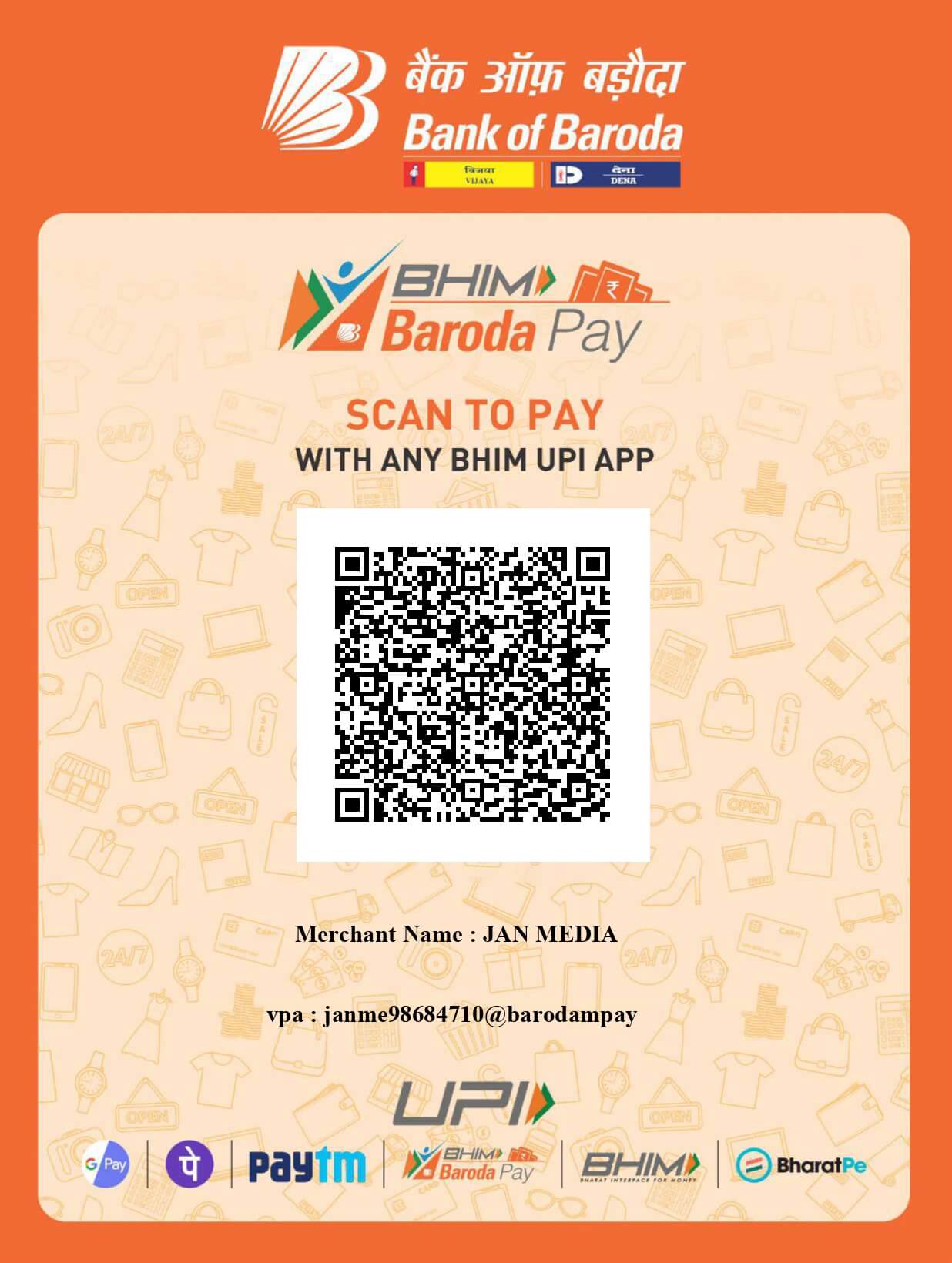‘इतिहास संबद्धता की मांग करता है।’ – विल्फ्रिड शीड
इस लेख का मकसद हिंदुस्तानी फिल्मी गीतों पर उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में विचार करना है। यह विचार भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति के प्रति रवैये को जानने, समझने और परिभाषित करने की कोशिश करते हुए किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह विश्लेषण ऐसे प्रबुद्ध समीक्षकों और इतिहासकारों को प्रेरित करेगा जो इन फिल्मों पर इस दृष्टि से विचार करने की योग्यता रखते हैं।
यह खासतौर पर गौर करने की बात है कि साउंड ट्रेक के आविष्कार के बिना हिंदुस्तानी फिल्म को वह मुकाम हासिल नहीं हो सकता था, जो उसे आज मिला हुआ है। पहली हिंदुस्तानी सवाक फिल्म आलमआरा 1931 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के प्रदर्शन होने के बाद से हिंदुस्तानी फिल्मों में संवाद और गानों की भरमार होती है। यह सच है कि फिल्म एक दृश्य माध्यम है लेकिन यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या हिंदुस्तानी फिल्में अपने वास्तविक अर्थों में फिल्में कही जा सकती हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में दृश्यात्मक आख्यान पर संवाद और गाने हावी रहते हैं। दरअसल, हिंदुस्तानी सिनेमा में संवाद भी ‘असंगीतात्मक’ गीत होते हैं। बहुत कम ऐसी हिंदुस्तानी फिल्में (बी आर चौपड़ा की फिल्म कानून को याद किया जा सकता है) होंगी जो बिना गीतों की होकर भी कामयाब रही हों। गीत हिंदुस्तानी फिल्मों का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है।
मुझे यकीन है कि इन गीतों की अंतर्वस्तु का विश्लेषण 1931 के बाद के भारतीय समाज के लोकाचार के बारे में महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाओं को उजागर करना चाहिए। यहाँ मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि स्त्रियों की सामाजिक-राजनीतिक दशा में चैंकाने वाले उलटफेर को मुख्य स्त्री गायकों की स्वर गुणवत्ता में बदलाव की सरसरी परीक्षा द्वारा उजागर किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि यह जांच बहुत सतही है। तीस के दशक की बहुत-सी स्त्री गायकों की आवाजें मुझे उपलब्ध नहीं हो सकी हैं कि मैं उन पर विचार कर सकूं। मुझे सिर्फ कानन देवी, बिब्बो और राम दुलारी की आवाजों के कुछ रिकार्ड ही सुनने को मिल सके हैं। फिर भी, ये कुछ रिकार्ड भी कुछ बातों को रखने में बाधक नहीं बनते जिनके आधार पर आगे अध्ययन किया जा सकता है।
मेरा मकसद हिंदुस्तानी फ़िल्मी गीतों के सामाजिक-राजनीतिक पहलुओं के बारे में सतर्कतापूर्वक अपने मत को रखना है। मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि आधुनिक आवाजों की तुलना में शुरुआती स्त्री गायकों की आवाजों में ज्यादा दृढ़ता थी। 1947 में आजादी (विभाजन) मिलने के बाद कम दृढ़ता वाली स्त्री आवाज में बदलाव अचानक दिखाई देने लगता है। विडंबना यह है कि आज़ादी मिलने के साथ ही स्त्रियों की सामाजिक-राजनीतिक दशा को नुकसान सहना पड़ता है। मैं इस दिशा में उठाए जा सकने वाले कुछ जरूरी कदमों का सुझाव भी दूंगा जिसके द्वारा स्त्रियों के दमन की बढ़ती प्रवृत्ति को उलटा जा सकता है।
गीत ‘संगीतमय’ कथन है। यह संवेदना से भरी भाषा है। गीत एक सूचना है-भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और अमूर्त। यह भावनाओं से भरी भाषा है। यह समझ में आने वाली बात लगती है कि मनुष्य प्रतीकात्मक भाषा को खोजे जाने के पहले से (शब्दहीन रागों में) ‘गाता’ था। गीत में प्रतीकात्मक विचार मेलोडी का माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह नहीं है कि मेलोडी से जुड़ा कथन मानव स्मृति में खासतौर पर जातीय स्मृति में बढ़ोतरी करता है।
मीडिया आलोचक और चिंतक मार्शल मेक्लुहान ने एक सूत्रवाक्य कहा हैः ‘माध्यम ही संदेश है।’ यह कथन भाषा के माध्यम की सूचनात्मक अंतर्वस्तु की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार मेलोडी स्वयं भी संदेश है। निस्संदेह यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों में अंतर्निहित है। संगीतकार मानते हैं कि राग ही नहीं बल्कि स्वर में भी दरअसल, मनोवैज्ञानिक/भावनात्मक अर्थ होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा जा सकता है कि मानव-स्वर की गुणवत्ता सूचना का महत्त्वपूर्ण वाहक है। हिंदुस्तानी फिल्म में यह बहुत सामान्य बात है कि एक ही अभिनेता के लिए एक ही फिल्म में दो-दो आवाजों (पाश्र्व गायकों)का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, बिमल राॅय की फिल्म मधुमती में दिलीप कुमार मुकेश और मोहम्मद रफी दोनों की आवाजों में गाते हैं। बहुत से लोगों को यह विचित्रता हास्यास्पद लगती है। दरअसल, इसमें कुछ भी न तो विलक्षण है और न ही हास्यास्पद। ऐसे मामलों में संगीत निर्देशक संगीतात्मक कथन के तथ्यों से ज्यादा उनमें निहित सत्यों में दिलचस्पी रखते हैं। एक प्रदत्त स्थिति में एक आवाज अधिकतम सूचना का वहन करने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है जबकि दूसरी आवाज दूसरे संदर्भ में ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। हिंदुस्तानी फिल्मी गीतों में आवाज की सूचनात्मक अंतर्वस्तु के सवाल पर अभी विचार किया जाना बाकी है।
आलमआरा के प्रदर्शन के बाद से संगीतात्मक सूचना की वाहक स्त्रियां रही हैं। यह तथ्य इस बात से साबित होता है कि लता मंगेशकर उन गायिकाओं में से है जिनके गाये गीत विश्व में सबसे अधिक रिकाॅर्ड किये गये हैं। निश्चय ही हिंदुस्तानी फिल्मों में पुरुषों को गाते हुए दिखाया जाना अरुचिकर नहीं माना जाता। फिर भी, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को ज्यादा गाते हुए दिखाया जाता है। वीर मर्दों को (मसलन, राजा, सेनापति और स्टंटमेन) अपवाद रूप में ही गाते हुए दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार स्टंट औरतों को भी गाते हुए नहीं दिखाया जाता। उदाहरण के लिए, नादिया (आमतौर पर प्रतिशोधात्मक वीरांगना, उसके हंटर का छुपा अर्थ क्या है?) को कभी गाते हुए नहीं दिखाया गया। महबूब खान की फिल्म आन में नादिरा तब तक नहीं गाती जब तक कि वह वीरांगना राजकुमारी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरती है और सती-सावित्री का रूप और वेश धारण करती है वैसे ही वह तुझे खो दिया गाने लगती है। यह गीत उसकी पराश्रित स्थिति का प्रमाण बन जाता है। सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी में महारानी गीत नहीं गाती; नहीं रज़िया सुलतान में रानी गुनगुनाती है। आमतौर पर इन फिल्मों में शाही मर्दों और औरतों के लिए गाने वाले बहुत से लोग होते हैं जिनमें कवि, दरबारी आदि शामिल हैं।
इस प्रकार हिंदी फ़िल्मों में भी गीत नज़ाकत, दुर्बलता और स्त्रीत्व से जुड़ी हुई चीज है। नारीत्व भी दुर्बलता है। तब यह विडंबनात्मक लगता है कि शास्त्रीय भारतीय संस्कृति में औरतों को धार्मिक गायन और नृत्य के लिए अयोग्य समझा जाता है। डांस ऑफ शिवा नामक वृत्तचित्र में बताया गया है कि धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े नृत्य में स्त्रियों की भूमिका पुरुष ही करते हैं। ऐसा क्यों है? जटिल भारतीय सामाजिक-आर्थिक श्रेणीबद्धता में आमतौर पर जो व्यक्ति गाता है वह अपने से ऊपर वाले के लिए गाता है। जब शक्तिशाली देवताओं की बात आती है तो उनके सामने भारतीय पुरुष शारीरिक और संगीतात्मक दोनों रूपों में आज्ञाकारी मुद्रा अपनाएगा। असल में, पुरुष देवताओं को बहला-फुसलाकर खुश करना चाहता है (हे प्रभु! मुझे मौत के मुंह से बचा, मुझे अमीर बना)। और निस्संदेह मनु के अनुसार जब धार्मिक कार्यों का सवाल आता है तो पुरुष का मुख स्त्रियों के मुख से ज्यादा पवित्र होता है।
मिरासी उत्तर भारत में गायकों और निष्पादकों के लिए प्रचलित अपमानजनक शब्द है। मिरासियों (पंजाबियों में इसके लिए और भी खराब शब्द कंज्जर इस्तेमाल होता है) का संबंध निम्न जाति से होता है। इस उपसंस्कृति में औरतों को गाने की आजादी थी। ‘गिरी हुई औरतों’ की इसी संस्कृति से शुरुआती महिला गायिकाएं (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) जुड़ी हुई थीं। ये गायिकाएं तथाकथित कोठा और मुजरा समाज का हिस्सा होती थीं। यह ‘प्रतिष्ठित’ उच्च भारतीय समाज का दूसरा स्याह पक्ष था। ठुमरी और दादरा की महान गायिकाएं मसलन, बेगम अख्तर, रसूलन बाई, गिरिजा बाई और दूसरी गायिकाएं इसी बाज़ार (या मुजरा) की देन थीं।
यहां तक कि ठुमरी और दादरा गाने वाली महिलाओं की गायकी भी पुरुषों द्वारा अधिग्रहीत किये जाने से बहुत दूर नहीं थी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि सर्वोत्तम ‘महिला गायकी’ भी कुशलता से पुरुषों- उस्ताद अब्दुल करीम खान (किराना घराना) और बड़े गुलाम अली खान (पटियाला घराना)- की संगत में ही संपन्न हुई है। इसका अतिवादी मामला फय्याज़ खान में देखा जा सकता है जिनका संबंध उस आगरा घराने से था जिनमें मर्दाना आवाज पर ज्यादा जोर था और जिन्होंने ठुमरी और दादरा को पुरुषों के लिए हड़प लिया।
यहां तक कि मुजरा गायकी में भी औरतों का प्रवेश आसान नहीं था। इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा था और इस बात को उनकी आवाज की गुणवत्ता में प्रचुर मात्रा में दर्ज है। इनमें से ज्यादातर गायिकाओं की आवाज अति संयमित और वज़नदार है। औरतों की आवाज पुरुष गायकों का अनुकरण करती थी। मलिका पुखराज (अब पाकिस्तान में) सादी और कठोर महिला गायकी की खास मिसाल है। ठुमरी और दादरा के एक स्थानीय (मेरा गृहनगरः टांगा, तंजानिया, पूर्व अफ्रीका) अधिकारी श्री ग़ुल राम मलिका पुखराज के गायन अभी तो मैं जवान हूं बजाया करते थे और कहते थेः ‘इस आवाज से तुम सारी रात प्यार करो। तुम हार जाओगे ये नहीं झुकेगी।’
साफ है कि वह पुखराज की आवाज में निहित काम्यता की ओर संकेत कर रहे थे। ठुमरी/दादरा की गायकी युद्ध के लिए तैयार आवाजें थीं। जब वे गाती थीं तो लगता था जैसे उनके मुंह से गोलियां निकल रही हों। यह युद्ध था। आदमी बचने के लिए भाग रहे थे। इस महान गायिकाओं के पास सख्त सम्मोहक आवाजें थीं। मुजरा माहौल में आदमी अपनी श्रेणीबद्धता को ‘घुटने मरोड़कर’ कायम रख पाता था। लेकिन इस मुद्रा में श्रेणीबद्धता को बनाए रखना भद्दा होता। कामना ने सबको बराबर कर दिया था और कर दिया है। कोठे पर आदमी और औरत के बीच बैचेन करने वाला युद्धविराम कायम था।
कोठे के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ थी वह ‘मादाम’ जो बैठी हुई अपने सरोते से सुपारी काटती रहती है। ‘आइए! तशरीफ रखिए। आपकी सुन्नत का वक्त आ गया। सुपारी दीजिए। सरोता तैयार है।’ यहां सुपारी काटने का मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत साफ है। यह सुन्नत का समय है। सुन्नत कुछ हद तक बधियाकरण है (बधिया होने की चिंता तो इसमें रहती ही है)।
तीस के दशक की फिल्म गायिकाएं आमतौर पर ऊंचे गले वाली थी। उनमें से कुछ (जैसे बेगम अख्तर) सबसे निचले स्वर से गाती थी। इनमें साफ अपवाद बिब्बो और काननदेवी थीं। वे दोनों काफी ऊंचे स्वर से गाती थी। हालांकि उनकी आवाजों में भी गुरुत्वाकर्षण की ताकत को मैं पहचान लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कानन देवी की आवाज भारी लहजे़ की जमीन पर टिकी होती थी। निश्चय ही बिब्बो और कानन देवी की आवाजें ‘छोटी’ आवाजें नहीं थीं।
चालीस का दशक हिंदुस्तानी फिल्मी गीत का प्रौढ़ता का काल था। इस दौरान गायकी का क्षेत्र ठोस आवाजों से भर गया। जैसे अमीरबाई कर्नाटकी, ज़ोहरा बाई अंबालावाली, मीना कपूर, खुर्शीद, सितारा आदि। खासतौर पर इस दौर की आवाजें थीं- नूरजहाँ, सुरैय्या और शमशाद बेगम।
पक्के तौर पर नूरजहाँ की आवाज ऊँचे स्वर वाली थी। उसकी आवाज में रंग, गीतात्मकता और नाटकीयता के तत्व समाहित थे। आज तक फिर ऐसी कोई फ़िल्मों की गायिका नहीं आई जिसकी आवाज का इतना विस्तृत आयाम और स्वरूप हो। इस बात को पहचानने के लिए ज़ीनत के दो गाने (आहे न भरीं; आजा री नींदिया) सुनना ही पर्याप्त है। उसकी गायकी ने उस ‘छोटी लड़की’ की आवाज को भी पैदा किया जिसे कि अभी आना था।
नूरजहाँ एक प्रच्छन्न मकड़ी की तरह थी जो कि पुरुष दंभ को फांसने के लिए मायावी जाल बुनती है। बहुत से संगीत निर्देशकों ने फ़िल्म गायकी में विभिन्न स्वर रणनीतियों की क्षमता को जांचने के लिए उसकी आवाज का इस्तेमाल किया। सुरैय्या की आवाज बंधी हुई आवाज थी जो सरल-सादे गीत गाने के लिए आदर्श थी। वह कलाविहीन गायकी की कला में माहिर थी। उसकी आवाज भी महीन नहीं थी। उसमें वज़न था। शमशाद बेगम की आवाज सख्त और तीक्ष्ण थी। मेला, बाबूल और नया अंदाज में उसे मुकेश, तलत महमूद और किशोर कुमार की तुलना में निर्णायक तीक्ष्णता बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही उसके साथ (चांदनी रात) स्वर से स्वर मिला पाता था। शमशाद की आवाज बहुत साफ, सख्त और नपी-तुली थी। वह गीत में उन्मादकता भर देती थी।
उन्नीस सौ चालीस के दशक के मुख्य पुरुष गायक जैसे कुंदनलाल सहगल, सुरेंद्र, जी.एम.दुर्रानी, अमर, करन दिवान आदि का महत्त्व कम होना स्वाभाविक था। सहगल खुद की ताकत दिया जलाओ (तानसेन) के बाद ही दिखा सके। इस दौर की सबसे मजबूत आवाज पंकज मलिक की थी जिनकी शैली बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अपनी मुद्रा कभी उत्तेजक नहीं बनने दी। सहगल के अपवाद को छोड़कर चालीस के दशक में गायिकाएं ही छाई रहीं। अपनी उग्रता में पुरुषों की तुलना में महिला गायकी एक-आध कदम आगे ही थी।
फ़िल्म गायिकाओं के बढ़ते कदम भारत के आजाद होने के साथ ही यकायक रुक गये। इस अचानक हुए बदलाव का कारण क्या था? खास बात यह है कि 1947 से पहले पुरुष स्त्रियों को जगह देने के लिए इतना उदार क्यों था? मेरा मानना है कि ब्रिटिश राज के धुंधलके में भारत की राजनीतिक घटनाओं ने इस परिवर्तन के लिए स्थितियां पैदा की थीं। इन घटनाओं को निम्न प्रकार से पेश किया जा सकता है।
हिंदुस्तानी फिल्म आलमआरा जिसमें पहली बार आवाज़ का इस्तेमाल हुआ उस समय बनी जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हो रहा था। यह पूर्ण स्वराज (1929) हासिल करने की दिशा में पहला आंदोलन था। हिंदुस्तानी फ़िल्म ने भी आवाज़ प्राप्त करने के साथ स्वतंत्रता का संकल्प लिया। मूक फिल्में यदि दृश्य रूप में अंतरराष्ट्रीय सिनेमा से जुड़ी थी, तो बाध्यकारी गीतात्मक आवाज के साथ जुड़कर हिंदुस्तानी फ़िल्म ने अलग रास्ता अपनाया।
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन के साथ आम जनता का जुड़ाव भी बढ़ता जा रहा था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में स्त्रियों की भागीदारी भी बढ़ रही थी। भारतीय स्त्रियों के लिए राजनीतिक अभिव्यक्ति के रास्ते इससे पहले तक बंद थे। लेकिन 1930 और 1940 के दशकों में ये उनके लिए ज्यादा खुले। सत्याग्रह में उग्र अहिंसात्मक प्रतिरोध निहित था। आश्चर्य नहीं कि औरतें- यहां तक कि फ़िल्म गायकी में भी अधिक उग्रता थी। आजादी की लड़ाई में औरतों को शामिल कर भारत ने अपनी यह इच्छा जता दी थी कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह कोई भी अतिवादी सामाजिक रास्ता (मसलन महिलाओं की महान आवाज़ को अनुमति देना) अपना सकता है।
15 अगस्त 1947 को भारत ने ‘पूर्णतः तो नहीं लेकिन तत्वतः’ (जवाहरलाल नेहरू) स्वाधीनता प्राप्त की। कई प्रमुख गायिकाओं (नूरजहाँ, खुर्शीद बेगम) की आवाज़ों से देश वंचित हो गया जो पाकिस्तान चली गई थी। दूसरी कई आवाज़ों (अमीरबाई कर्नाटकी, ज़ोहराबाई अंबालावाली और मीना कपूर) को मानो ग्रहण लग गया। सुरैय्या, शमशाद बेगम और राजकुमारी को छोड़कर गायिकाओं के मोर्चे पर अपेक्षाकृत खामोशी छा गयी। इस सन्नाटे ने पुरुषों को मौका दिया कि वे दोबारा संगठित हों और भविष्य के लिए नयी रणनीति अपनाए। आजादी हासिल हो चुकी थी और समय आ गया था कि औरतों को वापस रसोई में भेज दिया जाए।
यह जानना शिक्षाप्रद है कि दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान औरतों को ठीक इसी तरह के अनुभवों में से अमरीका और पश्चिमी यूरोप में भी गुजरना पड़ा। पुरुषों के युद्ध मोर्चे पर होने के कारण यह जरूरी हो गया कि औरतों को कारखाने चलाने और देश के अंदर देखभाल करने के लिए तैयार किया जाता। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो औरतों को मजबूर किया गया कि वे बाहर का काम (कम से कम कारखानों में काम करना ) छोड़ दें।
भारत में पुरुषों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छित और उत्साही किशोरी लता मंगेशकर के रूप में प्राप्त हुई। फिल्म गायकी में लता की आवाज के प्रवेश के साथ स्त्रियां एक बार फिर घर की ओर मुड़ गयीं।
लता मंगेशकर की आवाज को पेश करने का श्रेय उस्ताद गुलाम हैदर को था जिन्होंने बहुत साल पहले नूरजहाँ को भी पेश किया था। उन्होंने शहीद (1948) के लिए लता-मदनमोहन की युगल आवाज में एक गाना रिकार्ड किया था लेकिन फ़िल्म में उसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। इसकी जगह इस युद्ध संबंधी फ़िल्म में उन्होंने सुरिंदर कौर की सख्त आवाज का इस्तेमाल किया। फ़िल्म में दो भागों में रफ़ी और साथियों द्वारा गाया हुआ प्रभावशाली प्रयाण गीत- वतन की राह में- भी फ़िल्माया गया था। इस गीत में रफ़ी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाली आवाज है जो पुरुषों (नौजवां शब्द पर ध्यान दें) का (छुपे तौर पर) आह्वान करता है कि वे औरतों से आगे बढ़ें। सुरिंदर कौर की आवाज के आवरण में (औरतों को थोड़ी देर अंधेरे में रखा जाना था) मास्टरजी लता की आवाज को मजबूर (1948) में पेश करते हैं। उसी साल लता को खेमचंद प्रकाश जिद्दी में (याद करे चंदा रे) सामने लाते हैं। आइए, लता की आवाज पर विचार करें।
जब पहली बार लता की आवाज सुनाई गई तो उसके ध्वनि में नवीनता दिखायी दी। यह नवीनता जितनी दिखाई देती थी उतनी थी नहीं। यह नूरजहाँ की ‘छोटी लड़की’ की आवाज थी। यह प्रबलता और प्रचुरता से रहित ऊंचे सुर वाली आवाज थी। यह छोटी आवाज थी जो बहुत हल्के ढंग से बिना किसी तरह का प्रयत्न किए दक्षता से विचरण करती थी। इसमें पर्याप्त वजन था कि मेलोडी को निश्चित आकार दिया जा सके। पहली बात यह कि उसकी गायकी में वैविध्यता की क्षमता सीमित थी। बाद में, कुछ हद तक उसने इसका विकास किया। हालांकि यह वैविध्यता कभी भी नूरजहाँ की बराबरी नहीं कर पायी। इस मामले में वह अपनी छोटी बहन आशा भोंसले से कुछ हद तक पीछे ही थी। जहाँ पहले की गायिकाओं की आवाजों में एक तरह की उन्मादकता (दरअसल भावावेग) व्याप्त थी, वहीं लता की आवाज में ‘अकर्मकता’ की ध्वनि व्याप्त थी। उसकी आवाज़ में यौन के चिन्ह नहीं थे (और हैं)। वह तारुण्य से पूर्व की किशोर वय की आवाज़ प्रतीत होती है। लता की निर्मल आवाज ऐंद्रिकता को जगाने की बजाय आत्मा को जगाती है। यही नहीं वह स्त्री स्वर को बाल्योचित बनाती है। सम्मोहक आवाज़ का जादू आखिरकार टूट जाता है। स्त्री काम्यता की स्याह अराजक ताकत का सामना किये बिना पुरुष अब स्त्रियों के स्वर का अनुभव कर सकता था। उनकी दुनिया सुरक्षित थी। शुक्र है! बच गये!
1949 का साल लता मंगेशकर का साल था। वह यहां-वहां हर कहीं थी। दूसरी गायिकाओं और गायकों के लिए 1949 का साल ‘खतरे के साथ जीने का साल’ हो गया था। सभी खास-खास संगीतकार अचानक उसकी आवाज की जगह देने का प्रयत्न करने लगे। नौशाद की उस समय चार फिल्में (अंदाज़, चांदनी रात, दिल्लगी और दुलारी) आयीं। एक का संबंध सुरैय्या (दिल्लगी) से था; दूसरी का संबंध शमशाद बेगम (चांदनी रात) से था; तीसरी फिल्म लता और शमशाद के बीच (दुलारी) बंटी थी, लेकिन लता की आवाज उसमें छाई हुई थी और चैथी फ़िल्म जो नौशाद की सबसे महत्त्वाकांक्षी फ़िल्म (अंदाज़) थी उसमें सिर्फ लता थी। श्याम सुंदर की दो फ़िल्में (लाहौर और बाज़ार) लता मंगेशकर पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। खेमचंद प्रकाश की फ़िल्म महल में लता की आवाज राजकुमारी पर भारी पड़ रही थी। लता ने इसका शीर्षक गीत गाया था। सी. रामचंद्र की फिल्म पतंगा और नमूना में लता ने शमशाद के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। गजरे में अनिल विश्वास ने सुरैय्या के मुकाबले में उसे खड़ा कर दिया था और सुरैय्या के लिए तो यह उसकी गायकी का पटाक्षेप था। शंकर और जयकिशन ने बरसात में लता की आवाज का धमाकेदार इस्तेमाल किया। 1949 के अंत तक आते-आते भारतीय फ़िल्म उद्योग भारी आवाज़ों का कब्रिस्तान बन गया था। लता ने भारतीय नारी के पीछे की ओर लौटने की शुरुआत की। उसका नेतृत्व किया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर की दो मुख्य गायिकाओं आशा भोंसले और गीता दत्त पर भी बात करना जरूरी है। आशा की आवाज़ लता की तुलना में पर्याप्त छोटी और महीन है। आरंभ में उसकी आवाज़ का इस्तेमाल बच्चों (बूट पालिश) के लिए या नायिकाओं की ताबेदार सखियों के लिए किया जाता था। ओ.पी. नय्यर आशा को लता की छाया से मुक्त करके बाहर लाए और उसे मुक्त क्षेत्र प्रदान किया। नय्यर के साथ आशा ने आवाज के सूक्ष्म अंतरों की खोज की। खासतौर पर नय्यर उसकी आवाज में छुपी हुई उन्मादकता को बाहर ला पाये। शायद दूसरे संगीतकार सचिन देवबर्मन थे जिन्होंने आशा को अपनी गायकी की पूरी संभावना के साथ गाने की इजाज़त दी। दूसरे संगीताकारों ने आमतौर पर आशा की आवाज का इस्तेमाल मुजरा गीतों के लिए किया ताकि उसकी उन्मादकता का दोहन कर सकें। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आशा ने स्त्री स्वर को दुबारा कामत्व प्रदान किया । हालांकि यह चालीस के दशक की विस्मयकारी, उग्र काम्यता और ऊंचे गले वाली गायकी नहीं थी। इसके विपरीत यह सुरक्षित, नियंत्रित और निर्देशित की जा सकने वाली आवाज थी। आशा ने उन्मादकता तो प्रदान की लेकिन ऐसी जिसे आसानी से झेला जा सके। उसकी आवाज में स्वच्छ और सुवासित काम्यता थी। उसकी उन्मादकता की आवाज पर सदैव युद्ध विराम का सफेद झंडा लहराता (आत्मसमर्पण?) रहता था। मैं अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो आशा की आवाज सुनकर बंदूक में गोलियां भरने लगे। क्या कोई किसी की ‘छोटी बहन’ के नजदीक जा सकता है?
गीतादत्त की आवाज गहरी और गूंजभरी थी। वह ऐसी आवाज थी जो औरतों में आशा को दोबारा जगा सकने में सक्षम थी। लेकिन संगीतकारों ने इस आवाज़ को साजिशाना ढंग से नष्ट कर डाला। बुलो सी. रानी ने जोगन (1950) में गीता की आवाज़ का कई भजन गाने के लिए इस्तेमाल किया। इनमें रोने-धोने की शैली में गुहार की गयी थी। आगे वह बारबार ठुकराई और दुखी भारतीय नारी के दर्द को व्यक्त करने के लिए ही बुलाई जाती रही। वह जल्दी ही ‘आवाज की निरुपा राय’ बन गयी। निरुपा राय हारी हुई, दमित और दुखी भारतीय नारी का प्रतीक थी। ओ. पी. नय्यर (आर पार में) ने गीता दत्त की आवाज में निहित उन्मादकता को पहचाना। आमतौर पर नय्यर ने उसकी आवाज का इस्तेमाल पश्चिमपरस्त, लंपट, दुस्साहसी और कैबरे नाच करने वाली स्त्रियों के लिए किया। हालांकि सचिन देवबर्मन ने बाज़ी में उसकी आवाज़ में निहित उन्मादकता को उभरने दिया था (तदबीर से बिगड़ी हुई तक़दीर बना ले) इस प्रकार गीता दत्त की आवाज में निहित खंडित मनस्कता (डॉ. जैकिल और मिस्टर हाइड) की शुरुआत हुई। वह या तो माँ हो सकती थी या तवायफ। उसकी प्रतिभा के अपव्यय का प्रमाण उसके आखिरी गीतों में से इस एक गीत में देखा जा सकता हैः वक्त ने किया क्या हसीं सितम (कागज़ के फूल)। इस गीत में अब उद्विग्न माहौल दिखायी देता है। यह खोये हुए राजनीतिक अवसरों के विलाप का गीत है। अधिकतर संस्कृतियां स्त्रियों को दबाकर रखना जरूरी मानती है। यह काम अकेले आदमी के वश का नहीं है इसलिए वह इस काम में दूसरी औरत की मदद लेता है। आदमी को चालीस के दशक की सम्मोहक आवाज वाली गायिकाओं को परास्त करने के लिए लता, आशा और (रोने-धोने वाली) गीता की जरूरत है। इसके साथ ही, पुरुष को अपने बीच से भी ऐसी धमाकेदार पुरुष आवाजों की जरूरत थी जो उनके काम को पूरा कर सके।
मोहम्मद रफ़ी के रूप में उन्हें मर्दानगी से भरी आवाज मिली। संगीतकार श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच (1944) में पहली बार गवाया। उसी साल नौशाद ने पहले आप के एक अभियान गीत में (ध्यान दें!) उसकी आवाज़ का इस्तेमाल किया। 1945 में उसने ज़ीनत फ़िल्म के लिए एक बहुत ही प्यारा धीमे स्वर का गीत गाया। हम पाते हैं कि रफ़ी ने शाहजहां (1946) में छड़ी सहगल (रुही, रुही) के हाथ से ले ली है। लेकिन रफ़ी को जुगनू (1947) के युगल गीत- जहां बदला- से प्रसिद्धी मिली। खास बात यह है कि इस गीत में उसकी आवाज पर नूरजहां की आवाज हावी रहती है। रफ़ी को आगे बढ़ने का आदेश गुलाम हैदर से शहीद (1948) में मिला। रफ़ी की गायकी का अभियान उनकी मौत तक बरकरार चलता रहा। रफ़ी की आवाज़ की नकल करने वाले कई गायक (जैसे महेंद्र कपूर, अनवर और शब्बीर कपूर) रहे हैं लेकिन रफ़ी की ‘मौलिकता’ अंत तक कायम रही। रफ़ी के रूप में हिंदुस्तान में अब भी एक ऐसी आवाज़ थी जिसमें ताकत, लचीलापन और उग्रता का समावेश था। रफ़ी की आवाज़ में विशाल विविधता थी, गहराई थी और आघात करने की क्षमता थी। युगल गायकी में सिर्फ़ आशा ही उसका साथ देने में सक्षम थी। हालांकि उसमें उस हद तक लचीलापन नहीं था। रफ़ी का पंजाबी लहजा उसकी आवाज की उग्रता को बढ़ाता ही था। ऐसे में स्त्री क्या करे? जब रफी का आगमन हुआ तो स्त्रियों को पीछे हटना पड़ा। उसकी अद्भुत आवाज़ की वजह से उसका इस्तेमाल प्रायः राजनीतिक प्रतिगामिता के मकसद के लिए भी किया गया।
उन्नीस सौ चालीस के उत्तरार्द्ध और पचास के दशक के दो प्रमुख गायकों- मुकेश और तलत महमूद- पर टिप्पणी करना जरूरी है। मुकेश ने पहली नज़र (1946) से अपनी गायकी की शुरुआत सहगल का अनुकरण करते हुए की। लेकिन वह जल्दी ही अपनी विशिष्टता खोजने में कामयाब रहे। उसकी आवाज़ में गहराई और गूंज दोनों का समावेश था और गाने में स्फूर्ति व्यक्त होती थी। हालांकि उसकी आवाज़ में विविधता का अभाव था और उससे कोई डर नहीं पैदा होता था। तलत की आवाज़ बारीक, लरज़दार, नाजुक और उदासी से भरी थी। उसकी आवाज़ ऐसी गज़लों और गीतों के लिए बहुत उपयुक्त थी जिसमें भावुकता और अंतर्मुखीनता हो। उसकी आवाज़ में पीड़ा और पराजय की सरिता बहती है। बहुतों के अनुसार मुकेश और तलत दोनों की आवाजें क्षीण आवाजें हैं जो रफ़ी की धूमधड़ाकेदार आवाज़ के तहत संघर्ष करती दिखायी देती है। प्रत्येक गायकी रफी के पीछे-पीछे चलने की कोशिश करती है।
अमरीकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकसित देशों ने अपनी नागरिकों को जिनमें स्त्रियां भी शामिल हैं, संवैधानिक रूप से बराबरी के अधिकार दिये। फिर भी, पश्चिमी देशों में भी अभी तक औरतों को वे सभी अधिकार हासिल नहीं हैं जो पुरुषों को मिले हुए हैं। बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए स्त्रियों का संघर्ष आज भी अनवरत जारी है। सदियों से जारी लिंग संबंधी गैरबराबरी की परंपरा को खत्म करना आसान नहीं है। भारतीय संविधान औरतों को बराबरी के अधिकार देता है लेकिन पुरानी परंपराएं औरतों को अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोकती है। औरतों को आज्ञाकारी बनाए रखा गया है। भारतीय सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी तत्वों ने स्त्रियों की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। कुल मिलाकर हिंदुस्तानी सिनेमा प्रगतिशील रहा है। मसलन, इसने फ़िल्मों में काम करने के लिए औरतों को तैयार करने का साहसपूर्ण काम किया। बाद में यह कोई समस्या नहीं रही। इसके बावजूद फ़िल्मों में अब भी स्त्रियों को अनुवर्ती बनाए रखने के चतुराई भरे तरीके आजमाए गए हैं। शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों ने स्त्रियों की प्रगति के सवाल को फ़िल्मों में भी हमेशा जिं़दा रखा है। लेकिन उनके इस प्रयासों को गंदला करने के लिए प्रतिक्रियावादी (खासकर पुरुष) उनके व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देने वाले कुछ ऊपरी अंतर्विरोधों (विवाहित लोगों से विवाह करना) पर निगाह रखते हुए आनंदित होते हैं। इसका मकसद, यही प्रतीत होता है कि वे औरत की प्रगति को कमजोर कर सकें।
जानबूझकर या अनजाने पुरुष (निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गीतकार) स्त्रियों की प्रगति को विफल करने में भागीदार बनते हैं। विडंबना यह है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे स्त्रियों की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। संयोग से कुछ समस्यात्मक आवाजें या तो जा चुकी हैं या जाने को है।
बाद में, नयी आवाजें (अनुराधा पौडवाल हेमलता, वाणी जयराम) ज्यादातर लता के दायरे का ही अनुकरण करती नज़र आती है। उदाहरण के लिए वाणी जयराम जो इस दायरे से बाहर की आवाज़ है उसे ज्यादा अवसर नहीं मिले हैं। निस्संदेह, चित्रा सिंह की शानदार आवाज का उदाहरण दिया जा सकता है। इस गायिका जैसी महीन आवाज कभी-कभार ही सुनने को मिलती है। और अभी भी उसने अपनी आवाज की शक्ति (और आवेग) को बनाए रखा है कि वह जगजीत सिंह की प्रौढ़ आवाज (भारत और पाकिस्तान दोेनों में सम्मिलित रूप से सबसे समृद्ध आवाज़ कही जा सकती है- यह आवाज का खजाना है) का साथ दे सकती है। उसकी आवाज दूसरे दर्जे को अस्वीकार करती है। इस गायिका की आवाज में अजेय नारी शक्ति प्रकट होती है।
सीमा के उस पार, पाकिस्तान में भारत की तुलना में कहीं ज्यादा औरतों को दबाया गया है। सख्त आवाज वाली गायिकाएं इकबाल बानो, ताहिरा सैय्यद और दूसरी स्त्रियां बराबरी के लिए संघर्ष करती रही हैं। ऐसी आवाजें भारत में भी है। उन्हें सबके सामने आने का अवसर दिया जाना चाहिए। वे औरतों को गुलामी से और पुरुषों को दमन के अमानवीय बोझ से मुक्त करेंगी।
संदर्भ
De Bary, William T., 1958. Sources of Indian Tradition. New York : Columbia University Press.
Rangoonwalla Firoze, 1968. Indian Film Index. Bombay
Wheed Wilfred, 1978. The Good Words and other Words. New York: E. P. Dutton
Watspm, Francis. 1974. A Concise History of India. London : Thames and Hudson.
(इस आलेख के लिखने का उद्देश्य हिंदुस्तानी फ़िल्मी गीतों को उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में जांच कर अपने समाज में स्त्रियों की दशा के प्रति भारतीय रवैये को समझना और परिभाषित करना है। जानकारी के अभाव के कारण मैं अपने इस आलेख में दक्षिण भारत की भाषाओं के फ़िल्मी गीतों को शामिल नहीं कर पाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्लेषण को इन भाषाओं के अच्छे जानकार समीक्षक/इतिहासकार आगे बढ़ाएंगे। मैं राजू भरतन और श्री वी. ए. के. रंगा राव का आभारी हूँ उन्होंने ज्योति को जलाए रखा है। मैं श्रीमती विजयलक्ष्मी देसराम का भी आभारी हँू जिनके साथ मुझे इस विषय पर जीवंत बातचीत का मौका मिला। उन्हें लेख में कही गयी बातों से नहीं बल्कि कहने के ढंग से एतराज था। यह लेख श्री हरमंदिर सिंह ‘हमराज़’ को समर्पित है।)